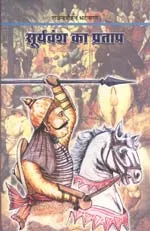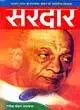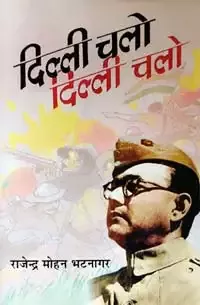|
जीवन कथाएँ >> सूर्यवंश का प्रताप सूर्यवंश का प्रतापराजेन्द्र मोहन भटनागर
|
32 पाठक हैं |
||||||
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के जीवन-संघर्ष पर आधृत उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
लोकतान्त्रिक अन्तश्चेतना, स्वतन्त्रता की अन्तर्भूत सृजना औ’
जिजीविषा की निर्बाध यशःयात्रा को मंगलैषणा तभी सम्भव है,
जबकि युद्ध की सघन अनवरतता बनी रहे।
मानवतामूलक मूल्यों तथा मान्यताओं की संस्थापना सहजजीवनीय उपस्थितियों की अनन्त गत्यभिमुखता औ’ विश्ववादी परिकल्पनाओं की संघर्षित यथार्थानुगतता तभी सम्भव है,
जबकि अन्तहीन युद्ध की अवचेतना की अनुभूति बनी रहे।
समग्र सामाजिक, अर्थविषयक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अहर्ताएँ औ’ नूतन सत्यानुसंधान की निकषीय अपरिहार्ताएँ तभी सम्भव हैं।
जबकि अथक, द्वन्द्वित औ’ अविराम युद्ध की स्वीकृति हमारे जीने का एकमात्र उद्दिष्ट हो।
इस उपन्यास की संदर्भित अन्तर्यात्रा का अभिलक्ष्य,
महाराणा प्रताप की सम्पूर्ण समग्रता औ’ विस्थापित व निरूपित मूल्यों का अभिचिन्तन ही।
इसकी संस्कारिता का प्रमुख अभीष्ट है।
जबकि युद्ध की सघन अनवरतता बनी रहे।
मानवतामूलक मूल्यों तथा मान्यताओं की संस्थापना सहजजीवनीय उपस्थितियों की अनन्त गत्यभिमुखता औ’ विश्ववादी परिकल्पनाओं की संघर्षित यथार्थानुगतता तभी सम्भव है,
जबकि अन्तहीन युद्ध की अवचेतना की अनुभूति बनी रहे।
समग्र सामाजिक, अर्थविषयक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अहर्ताएँ औ’ नूतन सत्यानुसंधान की निकषीय अपरिहार्ताएँ तभी सम्भव हैं।
जबकि अथक, द्वन्द्वित औ’ अविराम युद्ध की स्वीकृति हमारे जीने का एकमात्र उद्दिष्ट हो।
इस उपन्यास की संदर्भित अन्तर्यात्रा का अभिलक्ष्य,
महाराणा प्रताप की सम्पूर्ण समग्रता औ’ विस्थापित व निरूपित मूल्यों का अभिचिन्तन ही।
इसकी संस्कारिता का प्रमुख अभीष्ट है।
आस्था के स्वर
भारत के इतिहास में मध्यकालीन युग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विशेषतया यह
युग मुगल और मेवाड़ के संघर्ष और प्रेम का रहा है। जहाँ निरंकुश शासक अकबर
ने ‘आरोपित शासन’ को ‘सम्मति
शासन’ में बदल कर
राजतन्त्र को एक सर्वथा नवीन गरिमापूर्ण और उदारनीति की दिशा प्रदान की,
वहाँ मेवाड़ के महाराणाप्रताप ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए समग्र जीवन
समर्पित करने का अप्रतिम उद्धरण प्रस्तुत किया। यद्यपि इन तथ्यों के
सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है तथापि इन सबके उपरान्त भी न
महान् अकबर अपने पद से छोटा हो पाया है और न स्वतन्त्रता का अलख जगाने
वाला मेवाड़ पति महाराणा प्रताप अपनी गरिमा से तनिक पीछे हट सका है।
यथार्थतः सोलहवीं शताब्दी भारत के इतिहास में ऐसा संक्रांति–काल
सिद्ध हुआ है जिससे राष्ट्रीय और जन–जीवनीय चेतना में गंभीर और
सार्थक उद्वेलन हुआ है।
मैंने सोलहवीं शताब्दी को केन्द्र मानकर ‘महात्मा’ (कबीर), ‘महाबानो (रहीम), ‘श्यामप्रिया’ ‘न गोपी, न राधा, जोगिन’ (मीरा), ‘नीले घोड़े का सवारा आदि बहुत उपन्यास लिखे हैं। मीरा और महाराणा प्रताप पर मैंने तीन-तीन उपन्यास लिखे हैं—भिन्न कथा-वृत्त और भिन्न शैली में तीनों उपन्यासों के लिखने के पीछे भी भिन्न दृष्टि रही है। ऐसा मैंने ‘स्वान्तः सुखाय’ किया है। इसके लिए मैंने न सरकार का प्रश्रय चाहा है और न मेवाड़ राजवंश का। कारण, यह कार्य क्षिप्रता से तिरोहित होते मानवीय मूल्यों और ह्रासोन्मुखी चरित्र के कारण किया और उस जीवनाघारा से सम्बद्ध करने के लिए किया, जिससे वर्तमान टूटकर बिखर रहा है। मुझे लगा कि आज सत्य का कोई मूल्य नहीं है, आज निष्ठा और कर्मठता निरन्तर उपेक्षित होती जा रही है और आज संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इससे अनवरत जनजीवन खोखला होता जा रहा है और सत्ताभिमुखता की ओर युग बढ़ रहा है। मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहा है और हिंसा (जिसमें सत्ता का भी दबदबा सम्मिलित है) का मायवी साम्राज्य संवर्धित होता जा रहा है। मानव मानव रहे, वह महामानव बनने की कोशिश न करे, मेरे लिखने का अभिप्राय सदा यही रहा है।
आश्चर्य तब होता है जब मानव होने या सिद्ध करने की कथा को समीक्षक महामानव से जोड़ने लगते हैं। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सम्राट अकबर और स्वतन्त्रता का उद्भट योद्धा महाराणा प्रताप की समग्र गाथा भी मानव बनने की गाथा है। महामानव बनने का इतिहास नहीं। दोनों ने ‘सम्राटत्व’ की आरोपित गरिमा का ध्वंस किया है और दोनों ने जनजीवन से सम्बद्ध होने का प्रयास किया है। दोनों ने जनचेतना को अपने ढंग से प्रभावित किया है। वह मानव जो मानव होते हुए भी मानव नहीं है, जब अपने में से किसी को मानवोचित आधार पर जीने के लिए संघर्ष करता पाता है तब विचलित हो उठता है और उस पावन गंगा को जन-जीवन में न बहने देने के लिए प्रयास करता है। ‘महामानव’ उसी का प्रतिफल है। अन्ततोगत्वा मानव है क्या ! ‘सूर्यवंश का प्रताप’ इसी का उत्तर देने की चेष्टा-मात्र है।
‘सूर्यवंश का प्रताप’ को समीक्षक वह पाठकों ने अपनाया। उसे अपना स्नेह दिया। यथार्थतः ‘युद्ध’ न केवल महाराणा प्रताप के जीवन में था, प्रत्युत यह युद्ध उससे पूर्व भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। यह युद्ध मानव-मन में सदा चलता रहेगा। इस समय इस युद्ध की आग बहुत मद्धिम पड़ गयी है अतः मैंने महाराणा प्रताप के माध्यम से इस युग पर जम रही राख को हटाने की चेष्टा की है। इसमें भीलों की भूमिका को वही आदर दिया है जो महाराणा प्रताप को, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराणा की संघर्ष-प्रेरणा भील थे। यद्यपि मैं इसमें भीलों को विस्तार से चित्रांकित नहीं कर पाया हूँ तथापि जितना कर सकता था उतना मैंने अवश्य किया है।
इसके लिखने के पीछे मेरा मनतव्य यह रहा है कि मानव-कर्म की विविधतापूर्ण शैली से मानव को जोड़ कर एक मानवीय धारा प्रवाहित कर सकूँ। महाराणा प्रताप ऐसे मानव थे जो अपने अस्तित्व को तिरोहित नहीं होने देना चाहते थे। उनका संघर्ष हर उस सच्चे और निष्ठावान मानव का संघर्ष है जो उसे मानव होने के लिए सिद्ध करना होता है। हर एक का अपना अस्तित्व है। जब हर एक के अस्तित्व-बिम्ब को एक आँधी उखाड़ फेंकना चाहती है तब सहज महाराणा प्रताप की याद आने लगती है। वस्तुतः वह हमारे दुर्धर संघर्ष, निष्ठा, समर्पण और पराक्रम की अपूर्व धरोहर है। वह ऐसा इतिहास है जो कभी मर नहीं सकता। ऐसे भी अनेक प्रयास हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे जो महाराणा प्रताप की गरिमा को सन्देह की शय्या पर सुलाना चाहेंगे। वे यह भूल गये हैं कि अब महाराणा प्रताप का इतिहास मानव-जीवन का पर्याय बन चुका है और अब कोई भी ऐतिहासिक खोज उसे प्राप्त प्रतिष्ठा से अपदस्थ नहीं कर सकती।
मेरा उनसे विनम्र निवेदन है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपन्यासकार की दृष्टि महाराणा प्रताप पर ही अधिक केन्द्रित रही है, तत्कालीन जीवन पर कम। यह सच है क्योंकि मेरे लिए महाराणा प्रताप तत्कालीन जन-जीवन का प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप ने उदयसिंह के समय से उपेक्षा पायी थी और वह निरन्तर वह तकलीफों से घिरे रहे थे। हर बार सह-अस्तित्व की पहचान बनाये रखने के लिए, उन्हें जन-बल का आश्रय लेना पड़ा था, इसलिए सम्राट् होकर भी अकबर महाराणा प्रताप के जीतेजी मेवाड़ को नहीं जान सके और न कभी वे मेवाड़ जनजीवन की प्राणशक्ति बन सके। यह गहरी वेदना उन्हें अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक सालती रही। यही तो वह कारण है जो महाराणा प्रताप को सम्राट् अकबर की संघर्ष-शैली से सम्प्रक्त करता है और मानव-तुला पर उन्हें बहुत पीछे छोड़ जाता है। मेवाड़ का अस्तित्व सूर्य उनके समय इसलिए तिरोहित नहीं हुआ क्योंकि मेवाड़ का अस्तित्व मात्र प्रताप नहीं था प्रत्युत् समूचा जनजीवन था।
इस अवसर का लाभ उठाकर मुझे एक बात यहाँ और कहानी है और वह है इस कृति की रचना की भाषा को लेकर। इसमें मैंने भीलों और मेवाड़ियों की भाषा का प्रयोग नहीं किया है लेकिन मैंने उनकी संस्कृति, सभ्यता और सोच को भरपूर स्थान दिया है। आजकल यह एक परम्परा चल पड़ी है साहित्य को आंचलिक बनाने के लिए उनकी भाषा या बोली से उसे जोड़ा जाये। मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है। कारण, इससे बहुक्षेत्रीय हिन्दीभाषी जन को समझने में कठिनाई होती है। विशेषतया अहिन्दी भाषा-भाषियों के सामने हिन्दी को लेकर अनेक भ्रान्तियाँ पैदा होती हैं हिन्दी-विरोध का एक यह भी कारण है। मैं बोलियों और अंचल विशेष की भाषा के विरोध में कतई नहीं हूँ। जो साहित्यकार ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सम्पूर्ण कृति उनकी बोली या भाषा में आने दें और लिपी नागरी रखें।
इस कृति को और अधिक उपादेय बनाने में मूर्धन्य उपन्यासकार अमृतलाल नागर, डॉ. पूनम दैया, डॉ. बेनीमाधव, डॉ. उमर वार्ष्णेय, जैनेन्द्र कुमार, डॉ. विनोदशंकर वर्मा, डॉ. मालती शर्मा का विशेष योगदान रहा है। श्री बी.एल.सिंह ने इस कृति को अपने शोध का विषय भी बनाया है। उनके सुझावों को ध्यान में रखा है। एतदर्थ मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ।
अन्ततः मैं यह कृति अपने सुधी पाठकों और विद्वान् समीक्षकों को सौंप रहा हूँ कि वे इस कृति को अपना पूर्ववत् स्नेह-प्यार प्रदान करेंगे और अपने विचारों से मुझे अवगत करायेंगे। अस्तु;
मैंने सोलहवीं शताब्दी को केन्द्र मानकर ‘महात्मा’ (कबीर), ‘महाबानो (रहीम), ‘श्यामप्रिया’ ‘न गोपी, न राधा, जोगिन’ (मीरा), ‘नीले घोड़े का सवारा आदि बहुत उपन्यास लिखे हैं। मीरा और महाराणा प्रताप पर मैंने तीन-तीन उपन्यास लिखे हैं—भिन्न कथा-वृत्त और भिन्न शैली में तीनों उपन्यासों के लिखने के पीछे भी भिन्न दृष्टि रही है। ऐसा मैंने ‘स्वान्तः सुखाय’ किया है। इसके लिए मैंने न सरकार का प्रश्रय चाहा है और न मेवाड़ राजवंश का। कारण, यह कार्य क्षिप्रता से तिरोहित होते मानवीय मूल्यों और ह्रासोन्मुखी चरित्र के कारण किया और उस जीवनाघारा से सम्बद्ध करने के लिए किया, जिससे वर्तमान टूटकर बिखर रहा है। मुझे लगा कि आज सत्य का कोई मूल्य नहीं है, आज निष्ठा और कर्मठता निरन्तर उपेक्षित होती जा रही है और आज संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इससे अनवरत जनजीवन खोखला होता जा रहा है और सत्ताभिमुखता की ओर युग बढ़ रहा है। मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहा है और हिंसा (जिसमें सत्ता का भी दबदबा सम्मिलित है) का मायवी साम्राज्य संवर्धित होता जा रहा है। मानव मानव रहे, वह महामानव बनने की कोशिश न करे, मेरे लिखने का अभिप्राय सदा यही रहा है।
आश्चर्य तब होता है जब मानव होने या सिद्ध करने की कथा को समीक्षक महामानव से जोड़ने लगते हैं। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सम्राट अकबर और स्वतन्त्रता का उद्भट योद्धा महाराणा प्रताप की समग्र गाथा भी मानव बनने की गाथा है। महामानव बनने का इतिहास नहीं। दोनों ने ‘सम्राटत्व’ की आरोपित गरिमा का ध्वंस किया है और दोनों ने जनजीवन से सम्बद्ध होने का प्रयास किया है। दोनों ने जनचेतना को अपने ढंग से प्रभावित किया है। वह मानव जो मानव होते हुए भी मानव नहीं है, जब अपने में से किसी को मानवोचित आधार पर जीने के लिए संघर्ष करता पाता है तब विचलित हो उठता है और उस पावन गंगा को जन-जीवन में न बहने देने के लिए प्रयास करता है। ‘महामानव’ उसी का प्रतिफल है। अन्ततोगत्वा मानव है क्या ! ‘सूर्यवंश का प्रताप’ इसी का उत्तर देने की चेष्टा-मात्र है।
‘सूर्यवंश का प्रताप’ को समीक्षक वह पाठकों ने अपनाया। उसे अपना स्नेह दिया। यथार्थतः ‘युद्ध’ न केवल महाराणा प्रताप के जीवन में था, प्रत्युत यह युद्ध उससे पूर्व भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। यह युद्ध मानव-मन में सदा चलता रहेगा। इस समय इस युद्ध की आग बहुत मद्धिम पड़ गयी है अतः मैंने महाराणा प्रताप के माध्यम से इस युग पर जम रही राख को हटाने की चेष्टा की है। इसमें भीलों की भूमिका को वही आदर दिया है जो महाराणा प्रताप को, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराणा की संघर्ष-प्रेरणा भील थे। यद्यपि मैं इसमें भीलों को विस्तार से चित्रांकित नहीं कर पाया हूँ तथापि जितना कर सकता था उतना मैंने अवश्य किया है।
इसके लिखने के पीछे मेरा मनतव्य यह रहा है कि मानव-कर्म की विविधतापूर्ण शैली से मानव को जोड़ कर एक मानवीय धारा प्रवाहित कर सकूँ। महाराणा प्रताप ऐसे मानव थे जो अपने अस्तित्व को तिरोहित नहीं होने देना चाहते थे। उनका संघर्ष हर उस सच्चे और निष्ठावान मानव का संघर्ष है जो उसे मानव होने के लिए सिद्ध करना होता है। हर एक का अपना अस्तित्व है। जब हर एक के अस्तित्व-बिम्ब को एक आँधी उखाड़ फेंकना चाहती है तब सहज महाराणा प्रताप की याद आने लगती है। वस्तुतः वह हमारे दुर्धर संघर्ष, निष्ठा, समर्पण और पराक्रम की अपूर्व धरोहर है। वह ऐसा इतिहास है जो कभी मर नहीं सकता। ऐसे भी अनेक प्रयास हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे जो महाराणा प्रताप की गरिमा को सन्देह की शय्या पर सुलाना चाहेंगे। वे यह भूल गये हैं कि अब महाराणा प्रताप का इतिहास मानव-जीवन का पर्याय बन चुका है और अब कोई भी ऐतिहासिक खोज उसे प्राप्त प्रतिष्ठा से अपदस्थ नहीं कर सकती।
मेरा उनसे विनम्र निवेदन है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपन्यासकार की दृष्टि महाराणा प्रताप पर ही अधिक केन्द्रित रही है, तत्कालीन जीवन पर कम। यह सच है क्योंकि मेरे लिए महाराणा प्रताप तत्कालीन जन-जीवन का प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप ने उदयसिंह के समय से उपेक्षा पायी थी और वह निरन्तर वह तकलीफों से घिरे रहे थे। हर बार सह-अस्तित्व की पहचान बनाये रखने के लिए, उन्हें जन-बल का आश्रय लेना पड़ा था, इसलिए सम्राट् होकर भी अकबर महाराणा प्रताप के जीतेजी मेवाड़ को नहीं जान सके और न कभी वे मेवाड़ जनजीवन की प्राणशक्ति बन सके। यह गहरी वेदना उन्हें अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक सालती रही। यही तो वह कारण है जो महाराणा प्रताप को सम्राट् अकबर की संघर्ष-शैली से सम्प्रक्त करता है और मानव-तुला पर उन्हें बहुत पीछे छोड़ जाता है। मेवाड़ का अस्तित्व सूर्य उनके समय इसलिए तिरोहित नहीं हुआ क्योंकि मेवाड़ का अस्तित्व मात्र प्रताप नहीं था प्रत्युत् समूचा जनजीवन था।
इस अवसर का लाभ उठाकर मुझे एक बात यहाँ और कहानी है और वह है इस कृति की रचना की भाषा को लेकर। इसमें मैंने भीलों और मेवाड़ियों की भाषा का प्रयोग नहीं किया है लेकिन मैंने उनकी संस्कृति, सभ्यता और सोच को भरपूर स्थान दिया है। आजकल यह एक परम्परा चल पड़ी है साहित्य को आंचलिक बनाने के लिए उनकी भाषा या बोली से उसे जोड़ा जाये। मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है। कारण, इससे बहुक्षेत्रीय हिन्दीभाषी जन को समझने में कठिनाई होती है। विशेषतया अहिन्दी भाषा-भाषियों के सामने हिन्दी को लेकर अनेक भ्रान्तियाँ पैदा होती हैं हिन्दी-विरोध का एक यह भी कारण है। मैं बोलियों और अंचल विशेष की भाषा के विरोध में कतई नहीं हूँ। जो साहित्यकार ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सम्पूर्ण कृति उनकी बोली या भाषा में आने दें और लिपी नागरी रखें।
इस कृति को और अधिक उपादेय बनाने में मूर्धन्य उपन्यासकार अमृतलाल नागर, डॉ. पूनम दैया, डॉ. बेनीमाधव, डॉ. उमर वार्ष्णेय, जैनेन्द्र कुमार, डॉ. विनोदशंकर वर्मा, डॉ. मालती शर्मा का विशेष योगदान रहा है। श्री बी.एल.सिंह ने इस कृति को अपने शोध का विषय भी बनाया है। उनके सुझावों को ध्यान में रखा है। एतदर्थ मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ।
अन्ततः मैं यह कृति अपने सुधी पाठकों और विद्वान् समीक्षकों को सौंप रहा हूँ कि वे इस कृति को अपना पूर्ववत् स्नेह-प्यार प्रदान करेंगे और अपने विचारों से मुझे अवगत करायेंगे। अस्तु;
राजेन्द्रमोहन भटनागर
खुली पाती पाठकों के नाम
मित्रों, आज उपन्यास के साथ उसकी अन्तरयात्रा और उस यात्रा के
अन्तर्द्वन्द्वों को देने का फैशन आउट ऑफ डेट होता जा रहा है। परंतु मैं
उसे आवश्यक मानता हूँ। कारण; वस्तु के निर्माण की कहानी वस्तु से कम
महत्त्वपूर्ण नहीं होती है। निस्सन्देह उसका महत्त्व स्वयंसिद्ध है;
क्योंकि वस्तु के सृजन की कहानी व्यक्ति जानना चाहता है और वही कदाचित्
उसकी जिज्ञासा, उसके अहम् को तोष देती है।
कुछ बातें बड़ी अजीब-सी जीवन में उतर जाती हैं। उनके लिए व्यक्ति कभी स्वप्न में भी नहीं सोच पाता। मैं अब तक, यानी अब से पूर्व ऐसा नहीं सोचता था। बिना अनुभूत किए विश्वास बोलता भी तो नहीं है। बात दरअसल यह है कि सन् ’77 से उदयपुर जाने का सिलसिला शुरू हुआ। लगातार अब तक चलता रहा। और अन्त में मैं उदयपुर निवासी रह गया।
यह बात नहीं कि इससे पूर्व मैंने ऐसी यात्राएँ नहीं की हों। सम्पूर्ण हिमालय मैंने अपने में जिया है—जहाँ ट्रेन नहीं जा सकती और जहाँ बस, मोटर जीप आदि नहीं जा सकतीं। परन्तु राजस्थान में पच्चीस वर्षों से रहते हुए मेरी आँखों में वह सम्मोहन नहीं पाल सका, जो अकस्मात ’77 से शुरू हुआ और आज तक निरन्तर फैलता जा रहा है।
झीलों की इस नगरी की रूपाभा स्वयं में अनेक रहस्य-सृष्टियाँ बुनती और खोलती दृष्टिगोचर होती है। अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के साथ यह मेरा अनुभव नहीं हो रहा था—प्राचीनतम पर्वत की अनुभूति अवश्य इस बार पूर्वानुभवों से एकदम साम्पृक्त थी।
उदयपुर, चित्तौड़ आदि की यात्रा और उसके आसपास की यात्रा करते हुए मुझे अचानक महाराणा प्रताप और मीरा की चर्चाएँ घेर लेती हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी जरूर रहा हूँ—और अपने इतिहास-ज्ञान से मुझे सन्तोष है; परन्तु मुझे हमेशा लगा है कि इतिहास कागजों से बाहर वहाँ के चप्पे-चप्पे में बिखरा हुआ है, जहाँ की बातें आप पढ़ रहे हैं। हालाँकि डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव और प्रो. मिस गिब्स जैसे विश्वविख्यात इतिहासकारों का सान्निध्य मुझे मिला है और उनसे इतिहास के अध्ययन के विधि–विधान को समझा है। वह वास्तव में तत्कालीन इतिहास की अध्ययन-प्रक्रियाओं से सम्पृक्त है। फिर; यह इतिहास तो उदयपुर, चित्तौड़ और उसके चारों ओर के अंचल में बिखरा हुआ है यह जीवन इतिहास है। उसमें स्पन्दन है। उसे इस सम्पूर्ण अंचल विशेष में घूम-घूम कर और कुरेदा और जाना-समझा जा सकता है।
मैंने हर बार प्रथम श्रेणी में यात्रा की अतः कुछेक ही व्यक्तियों का सान्निध्य मिल पया। अभी मार्च, ’78 में जब यात्रा कर रहा था तब रेल का एक अधिकारी टकराया था, जो प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले मुसाफिरों से भेंट कर तत्सम्बन्ध में उनके विचार जान रहा था। उसकी जिज्ञासा के उत्तर में मैंने उसे बताया कि ‘‘मेरा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अर्थ होता कि उस एकान्त का इस्तेमाल लेखन के लिए करूँ। डॉ. अम्बेडकर का संशोधित संस्करण, मीरा तथा इस उपन्यास के अनेक अध्याय रेल-यात्रा की ही देन है। बहुत कुछ ‘सिद्ध पुरुष’ भी इसी तरह पूरा हुआ है।
लेखन के अतिरिक्त मेरा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का और कोई न तो मकसद है और न कोई अन्य बात, जैसे सुविधा। जोड़ने के लिए यह बात मुझे सीधे सामन्ती प्रभाव से सम्बद्ध कर सकती है और कदाचित् मेरा इन्कार भी, इस साफगोई के बाद मुझे बचा नहीं सकता। प्रत्युत् मैं जानता हूँ कि मैं एक मध्यम चित्त परिवार की यातनाओं से घिरा आम इन्सान हूँ, हजारों-हजार उन लोगों में से एक हूँ, जिनकी पहचान व्यक्ति नहीं भीड़ है।’’
खैर, इन यात्राओं में मुझे बहुत सारी सामग्री हाथ लगी। उसी के परिणामस्वरूप मैं छोटी सादड़ी और भीलों की दुनिया की सपन-नगरी के गलियारों तक जा सका-गलियारों जैसी बात शायद ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ उनकी अर्धनग्न देह के मिथकों की पहचान करने नहीं गया था। उरोजों का अढका होना उनके पूत मन को ही चिह्नित करता है। निस्सन्देह वासना देखने वाले की दृष्टि में है और उसके अन्तर्मन में है जहाँ से उसमें दृष्टि अर्थ लेती है। वासना जिसे दृष्टिबद्ध किया जा रहा है, उनकी अर्धनग्न देह नहीं है। उनमें फैला पहाड़ियों-सा भोलापन और उन पहाड़ियों पर उतर आया निश्छल सघन सपन उनकी सरलता को ही दीप्त करता है। वस्तुतया उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता मानवतावादी मूल्यों और उसकी संचेतना की सही अर्थों में सम्पोषक है। उनमें शहरी चालाकी नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महाराणा प्रताप ने स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए इन्हीं लोगों को तैयार किया था। कदाचित् किसी ने इन लोगों की चर्चा इस ढंग से नहीं की है।
फतेहसागर झील के सामने खुलता वह कमरा, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, निरन्तर नेहरू-गार्डन की (विशेषतया रात में) भव्यता को पेश करता रहता था। सहेलियों की बाड़ी से लेकर इस झील का अन्तर्मन सैलानियों (उनमें भी नव वर-वधुओं) को सदैव सम्मोहित करता रहा है। उनमें जीने की कम्पन्नमयी स्फूर्ति भरता रहा है। मैं सोचता हूँ कि आमंत्रण-सम्मोहन में कितना प्यार है। मुझे याद हो आता है कि महाराणा प्रताप ने झीलों के सम्मोहन और पहाड़ियों के आकर्षण से अपने को विमुक्त कर एक अन्तहीन युद्ध शुरू किया था और स्वतन्त्रता के अभिप्राय को अभिव्यक्ति देने के लिए उन वन्य जातियों को खड़ा किया था, जो अपने को युद्धविरत किए थीं। श्री राम ने भी तो वनवास के अन्तराल रावण से युद्ध करने के लिए इन्हीं वन्य जातियों को तत्पर किया था।
कुछ बातें बड़ी अजीब-सी जीवन में उतर जाती हैं। उनके लिए व्यक्ति कभी स्वप्न में भी नहीं सोच पाता। मैं अब तक, यानी अब से पूर्व ऐसा नहीं सोचता था। बिना अनुभूत किए विश्वास बोलता भी तो नहीं है। बात दरअसल यह है कि सन् ’77 से उदयपुर जाने का सिलसिला शुरू हुआ। लगातार अब तक चलता रहा। और अन्त में मैं उदयपुर निवासी रह गया।
यह बात नहीं कि इससे पूर्व मैंने ऐसी यात्राएँ नहीं की हों। सम्पूर्ण हिमालय मैंने अपने में जिया है—जहाँ ट्रेन नहीं जा सकती और जहाँ बस, मोटर जीप आदि नहीं जा सकतीं। परन्तु राजस्थान में पच्चीस वर्षों से रहते हुए मेरी आँखों में वह सम्मोहन नहीं पाल सका, जो अकस्मात ’77 से शुरू हुआ और आज तक निरन्तर फैलता जा रहा है।
झीलों की इस नगरी की रूपाभा स्वयं में अनेक रहस्य-सृष्टियाँ बुनती और खोलती दृष्टिगोचर होती है। अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के साथ यह मेरा अनुभव नहीं हो रहा था—प्राचीनतम पर्वत की अनुभूति अवश्य इस बार पूर्वानुभवों से एकदम साम्पृक्त थी।
उदयपुर, चित्तौड़ आदि की यात्रा और उसके आसपास की यात्रा करते हुए मुझे अचानक महाराणा प्रताप और मीरा की चर्चाएँ घेर लेती हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी जरूर रहा हूँ—और अपने इतिहास-ज्ञान से मुझे सन्तोष है; परन्तु मुझे हमेशा लगा है कि इतिहास कागजों से बाहर वहाँ के चप्पे-चप्पे में बिखरा हुआ है, जहाँ की बातें आप पढ़ रहे हैं। हालाँकि डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव और प्रो. मिस गिब्स जैसे विश्वविख्यात इतिहासकारों का सान्निध्य मुझे मिला है और उनसे इतिहास के अध्ययन के विधि–विधान को समझा है। वह वास्तव में तत्कालीन इतिहास की अध्ययन-प्रक्रियाओं से सम्पृक्त है। फिर; यह इतिहास तो उदयपुर, चित्तौड़ और उसके चारों ओर के अंचल में बिखरा हुआ है यह जीवन इतिहास है। उसमें स्पन्दन है। उसे इस सम्पूर्ण अंचल विशेष में घूम-घूम कर और कुरेदा और जाना-समझा जा सकता है।
मैंने हर बार प्रथम श्रेणी में यात्रा की अतः कुछेक ही व्यक्तियों का सान्निध्य मिल पया। अभी मार्च, ’78 में जब यात्रा कर रहा था तब रेल का एक अधिकारी टकराया था, जो प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले मुसाफिरों से भेंट कर तत्सम्बन्ध में उनके विचार जान रहा था। उसकी जिज्ञासा के उत्तर में मैंने उसे बताया कि ‘‘मेरा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अर्थ होता कि उस एकान्त का इस्तेमाल लेखन के लिए करूँ। डॉ. अम्बेडकर का संशोधित संस्करण, मीरा तथा इस उपन्यास के अनेक अध्याय रेल-यात्रा की ही देन है। बहुत कुछ ‘सिद्ध पुरुष’ भी इसी तरह पूरा हुआ है।
लेखन के अतिरिक्त मेरा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का और कोई न तो मकसद है और न कोई अन्य बात, जैसे सुविधा। जोड़ने के लिए यह बात मुझे सीधे सामन्ती प्रभाव से सम्बद्ध कर सकती है और कदाचित् मेरा इन्कार भी, इस साफगोई के बाद मुझे बचा नहीं सकता। प्रत्युत् मैं जानता हूँ कि मैं एक मध्यम चित्त परिवार की यातनाओं से घिरा आम इन्सान हूँ, हजारों-हजार उन लोगों में से एक हूँ, जिनकी पहचान व्यक्ति नहीं भीड़ है।’’
खैर, इन यात्राओं में मुझे बहुत सारी सामग्री हाथ लगी। उसी के परिणामस्वरूप मैं छोटी सादड़ी और भीलों की दुनिया की सपन-नगरी के गलियारों तक जा सका-गलियारों जैसी बात शायद ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ उनकी अर्धनग्न देह के मिथकों की पहचान करने नहीं गया था। उरोजों का अढका होना उनके पूत मन को ही चिह्नित करता है। निस्सन्देह वासना देखने वाले की दृष्टि में है और उसके अन्तर्मन में है जहाँ से उसमें दृष्टि अर्थ लेती है। वासना जिसे दृष्टिबद्ध किया जा रहा है, उनकी अर्धनग्न देह नहीं है। उनमें फैला पहाड़ियों-सा भोलापन और उन पहाड़ियों पर उतर आया निश्छल सघन सपन उनकी सरलता को ही दीप्त करता है। वस्तुतया उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता मानवतावादी मूल्यों और उसकी संचेतना की सही अर्थों में सम्पोषक है। उनमें शहरी चालाकी नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महाराणा प्रताप ने स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए इन्हीं लोगों को तैयार किया था। कदाचित् किसी ने इन लोगों की चर्चा इस ढंग से नहीं की है।
फतेहसागर झील के सामने खुलता वह कमरा, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, निरन्तर नेहरू-गार्डन की (विशेषतया रात में) भव्यता को पेश करता रहता था। सहेलियों की बाड़ी से लेकर इस झील का अन्तर्मन सैलानियों (उनमें भी नव वर-वधुओं) को सदैव सम्मोहित करता रहा है। उनमें जीने की कम्पन्नमयी स्फूर्ति भरता रहा है। मैं सोचता हूँ कि आमंत्रण-सम्मोहन में कितना प्यार है। मुझे याद हो आता है कि महाराणा प्रताप ने झीलों के सम्मोहन और पहाड़ियों के आकर्षण से अपने को विमुक्त कर एक अन्तहीन युद्ध शुरू किया था और स्वतन्त्रता के अभिप्राय को अभिव्यक्ति देने के लिए उन वन्य जातियों को खड़ा किया था, जो अपने को युद्धविरत किए थीं। श्री राम ने भी तो वनवास के अन्तराल रावण से युद्ध करने के लिए इन्हीं वन्य जातियों को तत्पर किया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book